(9 अगस्त, आदिवासी दिवस)
आदिवासी समाज के संकट, संघर्ष एवं संस्कृति की महागाथा : ग्लोबल गाँव के देवता
डॉ. हसमुख परमार
आधुनिक हिन्दी साहित्य पर एक विहंगम दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात
हुए बिना नहीं रहता कि आदिवासी समाज के विविध संदर्भों की उपस्थिति-अन्य विषयों की
अपेक्षा कम मात्रा में ही सही-इसमें बहुत पहले से ही रही है। पिछले दो-तीन दशकों
में तो इस विषय का काफी व्याप हुआ। आदिवासी एवं गैर आदिवासी सर्जकों द्वारा आदिवासी
समाज को केन्द्र में रखकर विपुल मात्रा में साहित्य लिखा गया है। हिन्दी साहित्य
के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि दलित और स्त्री
जीवन से जुड़े लेखन के साथ आदिवासी समाज जीवन ने भी साहित्य में अपनी केन्द्रीय एवं
महत्वपूर्ण जगह बनाई है। “यह संतोष की बात है कि हिन्दी साहित्य ही विविध विधाओं
के रचनाकारों ने हाशिए पर रहने वाले, जंगलों-पहाड़ों-कन्दराओं में
निवास करने वाले, नदियों-कछारों सुदूर जंगलों में उन्मुक्त रूप से सैर करने
वाले, आज की सभ्यता, जीवन शैली और उसकी चकाचौंध
से दूर रहने वाले आदिवासियों की तरफ नजरें इनायत करते हुए उन्हें अपने साहित्य का वर्ण्य
विषय बनाने में दिलचस्पी दिखाई है।”1 परंपरागत सीमित वर्ग-वर्ण के चित्रण एवं अन्य विषयों के दायरे से बाहर आकर इन
साहित्यकारों ने इस पिछड़े हुए एवं समाज की मुख्य धारा से काफी दूर रहे इस समाज के
सर्वांगीण रूप को अपनी लेखनी के जरिए हमारे सामने रखा। आदिवासियों की संस्कृति, इनके जीवन
संबंधी विविध प्रश्न, इनके साथ हो रहे अन्याय व शोषण आदि का दस्तावेजी चित्रण करने
के साथ-साथ इन साहित्यकारों के लेखन ने अनेक एतिहासिक आदिवासी अंदोलनों ओर संघर्षों
से ऊर्जा प्राप्त करके इस समाज को अपने अस्तित्व एवं अस्मिता हेतु संघर्षों को बल
प्रदान करते हुए इसमें चेतना का संचार तथा अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की
हिम्मत भी दी है। वैसे तो कविता, कहानी, नाटक जैसी विधाओं से संबंधी अनेकों रचनाओं में आदिवासी जीवन की तस्वीर दिखाई
देती है, किन्तु इस समाज के व्यापक फलक एवं उसके प्रति गहरी संवेदना
के मामले में अन्य विधाओं की तुलना में उपन्यास सबसे आगे व सबसे सशक्त विधा कही जा
सकती है।
आदिवासी
जीवन को लेकर लिखे गए उपन्यासों की परंपरा का प्रस्थान बिन्दु जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी
कृत ‘वसंत मालती’ उपन्यास को माना जाता है।
“आदिवासी जीवन संबंधी उपन्यास लिखने वालों में सबसे पहला नाम जगन्नाथ प्रसाद
चतुर्वेदी का लिया जाता है, जिन्होंने सन् 1899 में ‘वसंत मालती’ उपन्यास
लिखा जो मुंगेर जिले के मलयपुर अंचल के मल्लाह आदिवासी जीवन पर आधारित हैं।”2 उक्त विषय को निरूपित करने
वाले उपन्यासों की परंपरा को समृद्ध व सुदृढ़ बनाने में अनेक उपन्यासकारों का
योगदान रहा। मन्नन द्विवेदी, देवेन्द्र सत्यार्थी, योगेंद्र
नाथ सिन्हा, रांगेय राघव, नागार्जुन, रेणु, राजेंद्र
अवस्थी, शानी, श्याम परमार, हिमांशु
जोशी, राकेश वत्स प्रभृति रचनाकारों की कुछ औपन्यासिक कृतियों में
आदिवासी समाज का प्रतिबिंब दिखता है। आगे चलकर आठवें-नौवें दशक में दलित एवं स्त्री विमर्श के अतिरिक्त
आदिवासी विमर्श भी उभरकर आया, अतः पिछले दो-तीन दशकों में
आदिवासी जीवन केंद्रित उपन्यासों में आदिवासी विमर्श अच्छी तरह व्याख्यायित हुआ।
इस समयावधि में आदिवासियों की समस्याओं को चित्रित करने वाले उपन्यासकारों की
परंपरा के प्रमुख हस्ताक्षरों में संजीव, मनमोहक पाठक, वीरेंद्र
जैन, श्री प्रकाश मिश्र, मैत्रेयी
पुष्पा, तेजिंदर, भगवनदास मोरवाल, राकेश
कुमार सिंह, भालचन्द्र ओझा, विनोद कुमार सिंह, रामदीन
पाण्डेय, कान्हजी तोमर, श्रीमति अजित गुप्ता, पीटरलाल
एक्का, गुरवचन सिंह, शशिकलाराय आदि विशेष
उल्लेखनीय हैं। इसी पंक्ति में एक महत्वपूर्ण नाम है – रणेन्द्र और उनका
उपन्यास ‘ग्लोबल गाँव के देवता’।
भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ‘ग्लोबल
गाँव के देवता’ (सन् 2009) महज सौ पृष्ठों का यह उपन्यास रणेन्द्र की
प्रथम औपन्यासिक रचना है। इसमें झारखंड की जमीन और वहाँ के निवासी असुर समुदाय की
कथा वर्णित है। उपन्यास आकार की दृष्टि से भले ही लघु कहा जाए, किन्तु
इसमें एक आदिवासी समुदाय की प्रकृति, प्रवृत्ति एवं उनके साथ हो
रहे अन्याय की जो कथा वर्णित है वह किसी महागाथा से कम नहीं कही जा सकती। रणेद्र
झारखंड के आदिवासी समाज के अध्येता हैं। इन्होंने “झारखंड इन्साइक्लोपीडिया के चार
खंडो का भी संपादन किया। झारखंड इन्साइक्लोपीडिया
आदिवासियों की गाथा है। इसमें रणेन्द्र ने आदिवासियों की संस्कृति, प्रकृति, जंगल, पहाड़, इन पर हो
रहे अन्याय-अत्याचार तथा शोषण का चित्रण इस झारखंड इन्साइक्लोपीडिया में किया है।” लेखक का अपने इस उपन्यास में वर्णित झारखंड के
असुर समुदाय का प्रत्यक्षदर्शी रहना। “रुमझुम - लालचन (उपन्यास के पात्र) के साथ तीन साल जीवन
जीने-समझने की कोशिश की थी। हफ्तों, दिन-रात साथ गुजारे। लेकिन
उस वक्त सपने में भी यह ख्याल नहीं आया कि इस जिए हुए को किसी रचना में ढालना है।”3 इसके अतिरिक्त उपन्यास में आदिवासी समाज संबंधी विविध कहानियाँ,
जनश्रुतियाँ, विविध इतिहास ग्रंथ अन्य पुस्तकें, पुरातत्त्ववेत्ताओं
एवं मानवशास्त्रियों का रिसर्च आदि के उल्लेख से प्रमाणित होता है कि लेखक को
सिर्फ झारखंड के असुर समाज के वर्तमान का ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज का इतिहास
एवं इसके राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संदर्भों का ज्ञान भी विस्तृत है।
उपन्यास के
केन्द्र में भले ही असुर समाज का वर्तमान हो किंतु इसके निरूपण के साथ-साथ उपन्यास
आदिवासी समाज के ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संदर्भों से जुड़ता है।
“वैदिक काल से लेकर सुदूर अमेरिका में असुर संस्कृति का जो हश्र हुआ, उसमें अद्भुत
समानताएँ ऐतिहासिक आधार के साथ दिखाई गई है। किस प्रकार 1607 में अमेरिका के
वर्जीनिया प्रांत में अंग्रेजों ने जेम्स टाउन नामक पहली बस्ती बसाकर वहाँ के मूल
निवासी रेड इंडियन्स को धकेलकर किस प्रकार जनजातियों का लगभग सफाया कर दिया, उसका
वर्णन प्रथम बार प्रस्तुत कर उपन्यास अपने इस आधार को दृढ़ बनाता है कि इसी प्रकार यहाँ
कोयलाबीघा ओर भौंरापाट में जनजातीय संस्कृति ओर जीवन शैली को समाप्त कर उन्हें
भूमंडलीकरण का दानव पूरी तरह लील रहा है।”4 लेखक ने बहुत कलात्मक ढंग से मूल कथा की
देशबद्धता व कालबद्धता को बनाये रखते हुए असुरों की गाथा को एक सार्वकालिक एवं
सार्वदेशिक संघर्षगाथा के रूप में पेश किया है।
उपन्यास का
शीर्षक जितना आकर्षक है उतना सार्थक भी। उपन्यास की मूलसंवेदना व इसमें
वर्णित-स्थिति मूलत: भूमंडलीकरण की देन है। रचना में दो पक्षों – एक बहुराष्ट्रीय
कंपनियों के मालिक, व्यापारी, इनके दलाल हैं जिन पर सत्ता
पक्ष की भी कृपा बनी रहती है। दूसरा
झारखंड राज्य के भौंरापाट, सखुआपाट, पाथरपाट, क्ंदापाट
आदि गाँवों का निवासी आदिवासी समाज। इन दोनों पक्षों के बीच का संघर्ष और इस संघर्ष
में जद्दोजहद करते, पराजित होते आदिवासी समाज की त्रासदी केन्द्र में है। टाटा, वेदांग, शिंडालिको
जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, इनके मालिक यही तो ग्लोबल
गाँव के देवता हैं। लेखक ने जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है इसका सूत्र बहुत प्राचीन व
व्यापक संदर्भ से जोड़ा है। असुर जाति के आदिवासियों की कड़ी प्राचीन एवं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय
स्तर तक पहुँचती है। लेखक आदिवासी समुदाय के प्रति संवेदना व सहानुभूति रखते हुए
इस जाति विशेष के लोगों की संस्कृति, समस्याओं, विडंबनाओं
से हमें परिचित कराते हुए इनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षों को उजागर करते हैं और इस समाज को अपनी साज़िशों का शिकार
बनाने वाले देवताओं का असली रूप सामने लाते हैं। “जहाँ झारखंड के आदिवासियों की
कड़ियाँ वे इंका, माया, एक्टेक, रेड
इंडियन्स, भारतीय राक्षसों से जोड़ पाते हैं, वही आज के
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों की कड़ियाँ यूरोपीय शासकों एवं भारतीय देवताओं से।
रणेन्द्र शिकारी सत्ता के पक्ष से नहीं, बल्कि सत्ता के शिकार हुए
लोगों के पक्ष में खड़े होकर अपना उपन्यास रचते हैं। शिकार करने वाले देवताओं की वे
कलई तो खोलते ही है, लेकिन साथ ही साथ शिकार होने वाले आदिवासियों की खुद्दारी, जिजीविषा, प्रतिरोध, अटूट
विश्वास, संघर्ष में सतत पराजित होते चले जाने की करूण गाथा भी
लिखते है।”5
उपन्यास का
प्रमुख पात्र शिक्षक, जो उपन्यास का सूत्रधार हैं। प्रखंड कोयला विघा के भौंरापाट
की पीटी जी गर्ल्स रेजिडेंसियल स्कूल में उनकी पोस्टिंग होती है। वहाँ रहते हुए यह
शिक्षक इस क्षेत्र के असुर समाज के व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन से जुड़ते हैं और उनके
पक्षधर बन जाते है। इसी शिक्षक के माध्यम से असुर समाज की संघर्ष कथा उपन्यास में
प्रस्तुत हुई है। भाषा विज्ञान के अध्येता को इस बात का ज्ञान अवश्य होगा की हमारे
शब्द कोश में ‘असुर’ शब्द पहले तो देवतावाची था।
ऋग्वेद की आरंभ की ऋचाओं में यह देववाची शब्द है, पर बाद
में राक्षसवाची हो गया।
अतः आज
असुर शब्द सुनते ही हमें दैत्य या राक्षक का ही बोध होता है। जिसकी पहचान एक भयावह
डरावने रूपरंग वाले व्यक्ति के रूप में होती है। उपन्यास का सूत्रधार शिक्षक के मन
में भी यही धारणा रही है किन्तु जब लालचन असुर नामक व्यक्ति इनके सामने आता है तब
इनकी असुर संबंधी प्रचलित धारणा टूटती है – “सुना तो था कि यह इलाका असुरों का है
किन्तु असुरों के बारे में मेरी धारणा थी कि खूब लम्बे चौड़े, काले-कलूटे, भयानक दाँत-बाँत
निकले हुए, माथे पर सिंग-विंग लगे हुए होंगे। लेकिन लालचन को देख कर
सब उलट-पुलट हो रहा था। बचपन की सारी कहानियाँ उलट घूम रही थी।”6 इतना ही नहीं एतवारी को देखकर भी
शिक्षक को अपनी धारणा पर शर्म आ रही थीं। “यह छरहरी – सलोनी एतवारी भी असुर ही है, यह जानकार
मेरी हैरानी बढ़ गई थी। हप्ताभर से उसे देख रहा हूँ, न सूप
जैसे नाखून दिखे, न खून पीने वाले दाँत। कैसी कैसी गलत धारणा। खुद पर ही
अजब-सी शर्म आ रही थी।”7 लेखक का मूल
उदेश्य तो असुर नामक इस आदिवासी जनजाति की संघर्षकथा बताना है किन्तु इसकी जड़ें तो
वे प्राचीन भारतीय राक्षसों में देखकर दोनों की दशा-दिशा में समानता दिखाते हैं।
देवता तो पौराणिक इंद्र आदि देवता है किन्तु लेखक बात करते है – ग्लोबल गाँव के
देवताओं की, इनका संबंध भी पौराणिक देवताओं से जोड़कर। आज भी जारी
सुर-असुर संघर्ष को दिखाते है। इस संघर्ष में असुर का अंत भले ही सुनिश्चित हो
किन्तु अंतिम साँस तक लड़ना जरूरी है। “खनन कंपनियों की शाश्वत उपस्थिति मानो गर्दन
पर इंद्र की नंगी तलवारें। पुराने मिथ को नए अर्थ में प्रस्तुत करने की कला दिखाई
देती है।
इक्कीसवीं
सदी की पहचान विकास की सदी के रूप में हो रही है। समाज के हर वर्ग व वर्ण के
सर्वांगीण विकास की खूब बातें होती है। सरकार की ओर से अनेक कानून एवं विकास
योजनाओं के तहत विशेषतः पिछड़े हुए समाज को शिक्षा तथा रोजगार मुहैया कराने, इनकी जमीन, संस्कृति, पारंपरिक
व्यवसाय को सुरक्षित रखते इनके अस्तित्व को बचाये रखने के प्रयास तो हो रहे हैं।
बावजूद जरूरतमंद समाज क्यों अपने अधिकारों व बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रह जाता
है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। सत्य को खोजना, सच्चाई को
लाना वैसे भी संवेदना, सहानुभूति, महेनत, अध्ययन
एवं साहस के बिना संभव नहीं है। जहाँ तक आदिवासी समाज का संदर्भ है तो इस समाज को
देखने पर यह प्रश्न उठना लाज़मी है की देश को आजादी मिले आज कितने वर्ष हो गए, इस लंबी
समायावधि में क्या सही मायने मे इस समाज का विकास हुआ है ?
शताब्दियों से एक जैसी रही स्थिति में आज क्या कोई बुनियादी परिवर्तन हुआ है ? प्रस्तुत उपन्यास में इन प्रश्नों पर बहुत गंभीरता से विचार करते हुए
वास्तविकता पर से परदा उठाया गया है। इतिहास गवाह है कि यह समाज पहले से ही
उपेक्षित रहा, समाज की मुख्य धारा से अलग, अन्याय, शोषण का शिकार
और यह स्थिति आज भी बरकरार है। नये-नये तरीकों, तरह-तरह
की सुनियोजित साजिशों के चलते इनकी स्थिति और दयनीय होती जा रही है। “आदिवासी समाज
की ओर एक नजर डाले तो पता चलता है कि इन्हें पहले भी खदेड़ा जाता था और आज भी खदेड़ा
जा रहा है। यह खदेड़ना सदियों से चालू है। केवल रूप या तरीका बदल गया है। आखिर कब
तक और कहाँ तक पीछे हटा जाए ? यह एक सवाल है जो बार-बार
उपन्यास में आदिवासियों द्वारा सुनाई पड़ता है। उपन्यास के पात्र रुमझुम के शब्दों में हम वैदिककाल के सप्तसिंधु के
इलाके से होते हुए इस वर्ण-प्रांतर, कीकट, पैड्रिक, कोकराह या चुटिया नागपुर पहुँचे। हजारों सालों में कितने
इन्द्रों, कितने पांडवों, कितने सिंगबोगा ने
कितनी-कितनी बार हमारा विनाश किया, कितने गढ़ ध्वस्त किए उसकी
कोई गणना किसी इतिहास में दर्ज नहीं है, केवल लोककथाओं और मिथकों में
हम जिंदा है।”8
वर्तमान
में औद्योगिक विकास के नाम पर, जंगली जानवर के रक्षण के
बहाने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आदिवासियों की खनिज से भरी
जमीन की खुदाई की वजह से वह समाज विस्थापन का शिकार हो रहा है। अपने अस्तित्व को
बचाए रखने में संघर्षरत इस जाति की दशा व दिशा काफी चिंताजनक है। आग और धातु की
खोज द्वारा कभी इस जाति ने मानव सभ्यता के इतिहास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया
था किन्तु आज स्थिति यह है की यह समाज अपनी संस्कृति , जमीन, भाषा, अपनी
पहचान को सुरक्षित रखने में काफी जद्दोजहद कर रहा है। ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ में
इस स्थिति का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। सत्ता और समृद्धि ने-इस समाज के साथ
अन्याय किया है, जिसका सिलसिला बहुत पुराना है। “जब इन्होंने जंगलों की
रक्षा करने की ठानी तो इन्हें राक्षस कहा गया। जब इन्होंने अपनी पहचान की खातिर
भूमि और वन्य सम्पदा को सुनियोजित रूप से बर्बाद करने वाली नीतियों का विरोध किया
तो दुष्ट दैत्य कहलाए।” संस्कृति और सत्ता का यह युद्ध देवराज इन्द्र के जमाने से
लेकर ग्लोबल गाँव के देवताओं तक के युग में जारी है । लेकिन वैदिक युग के हजारों
हजार इंद्र से भी ग्लोबल गाँव के देवता ज्यादा शक्तिशाली निकले तभी तो जो तब नहीं
हुआ, आज वो हो रहा है।
औद्योगीकरण
एवं उदारीकरण के कारण आज बड़ी-बड़ी कंपनियों ने इस समाज के व्यवसाय को, इनकी आजीविका
की आधार बनी कला-कारीगरी को ही खत्म कर दिया। वैश्वीकरण के दौर में ग्लोबल गाँव के
देवता रूपी टाटा जैसी कंपनियों ने तो असुरों के लोहा गलाने और औजार बनाने के हुनर
का अन्त कर दिया है। इसलिए असुर मानते हैं कि टाटा कंपनी ने उसका जो विनाश किया वह
असुर जाति के अपने पूरे इतिहास में सबसे बड़ी हार थी। इस बार कथा-कहानी वाले
सिंग-बोंगा ने नहीं टाटा जैसी कंपनियों ने
हमारा नाश किया। उनकी फैक्टरियों में बना लोहा, कुदाल, खुरपी, गैंता, सुदूर हाथों
तक पहुँच गए। हमारे गलाये लोहे के औजारों की पूछ खत्म हो गई। लोहा गलाने का
हजारों-हजार साल का हुनर धीरे-धीरे खत्म
हो गया।
जो क्षेत्र खनिज संपदा से बहुत ही समृद्ध है वहाँ राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय
कंपनियों द्वारा सरकार की मदद से खनीज की खुदाई होती है। इस कार्य से इन क्षेत्रों
के स्थानीय निवासियों को मजदूरी तो मिलती है किंतु दूसरी ओर इन्हें विविध प्रकार
की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। खनन क्षेत्रों के स्थानियों लोगों की
दुर्दशा पर कुछ उपन्यासकारों ने कलम चलाई है। ग्लोबल गाँव के देवता में यह विषय
केन्द्र में रहा है। खनिज संपत्ति से भरपूर छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा की भूसम्पदा
का बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जिस रूप में दोहन कर वहाँ नव धनाड्य वर्ग को यदि एक
ओर स्वर्ग-सुखों से एक भोगमय ऐश्वर्य युक्त संसार दिया है तो दूसरी ओर वहाँ की
जन-जनातियों, मूल निवासियों को एक नरक की दुनिया दे डाली है। इधर हिन्दी उपन्यास में
इस क्षेत्र के उपन्यासकारों का ध्यान अपने चारों और पसरे इस भयावह यथार्थ की ओर गया
है। कोयला खदानों के जीवन पर पहले संजीव के ‘सावधान नीचे आग है’ और ‘धार’ जैसे
उपन्यास आए हैं किन्तु इस दशक (इक्कीसवीं सदी का प्रथम दशक) में झारखंड के खनन
क्षेत्र पर अनवर सुहैल का ‘पहचान’ और रणेन्द्र का उपन्यास ‘ग्लोबल गाँव के देवता’
आए है जो यहाँ के मूल निवासियों की व्यथा कथा को अपनी-अपनी दृष्टि से विश्लेषण करते
है।”10 रणेन्द्र ने अपने इस उपन्यास में झारखंड के खनन क्षेत्रों के
आदिवासियों के त्रासद जीवन को समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषित किया है।
महामारी, विस्थापन, स्त्रियों का जातीय शोषण जैसी समस्याओं की उपज इस खनन क्षेत्र
में हो रहे खनन कार्य से जुड़ी है।
ग्लोबल कंपनियाँ जमीन की खुदाई करके बॉक्साइट तो निकालकर ले
जाती है किंतु खुदाई के बाद गड्ढों को भरने की ओर इन कंपनियों द्वारा ध्यान नहीं
दिया जाता। खुले छोड़े गए यह गड्ढे स्थानीय लोगों के लिए वहुत बड़ी मुसीबत बन गए
क्योंकि इन गड्ढों में पनपे मच्छरों के कारण जो बीमारियाँ फैलती है। यहाँ तक कि जो
जाने जाती है, जिसकी मात्रा तो यहाँ चलनेवाले अन्धविश्वासों से होने वाली
हत्याओं से भी ज्यादा कही जाएँगी। डॉ. रामकुमार उपन्यास के सूत्रधार शिक्षक को
बताते हैं “एक तरफ इन खानों ने मजूरी तो दी तो दूसरी तरफ बर्बादी के सरंजाम भी खड़े
किए है। पिछले पच्चीस-तीस सालों में खान मालिकों ने जो बड़े-बड़े गड्ढे छोड़े हैं बरसात
में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और मच्छर पलते हैं। सेरेव्रेल, मलेरिया यहाँ के
लिए महामारी है।”
इन कंपनियों के मालिकों पर सरकार भी मेहरबान है, तभी तो वह
आम आदमी की समस्याओं के निवारण में दिलचस्पी नहीं ले रही। व्यापारियों और तथाकथित
सत्ता के सौदागरों की मिलीभगत से यह समाज इस हद तक कुचला जा रहा है कि इन्हें अपनी
ज़मीन से भी हाथ धोने को विवश होना पड़ता है। सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही, ऐग्रीमेंट
होता है कि बॉक्साइट निकालकर गड्ढा भरना है किंतु वैसा वास्तव में होता नहीं है।
पूरे पाट पर फैले इन सैकड़ों विशाल गड्ढों का क्या! ऐग्रीमेंट की पहली शर्त है कि बॉक्साइट
निकालकर गड्ढा भरना है, तो बीसों साल से क्यों नहीं
हो रहा यह काम ? हमें तो लगता है कि जान-बूझकर सरकार भी मटिया रही है।
चाहती है – पाट पर आबादी जितना जल्दी खत्म हो बॉक्साइट निकालने में उतनी ही आसानी
होगी।“12
नवउदारवादी अर्थव्यवस्था के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों के
व्यापार चक्र में देश के कई इलाके व वहाँ का समाज अपनी जमीन व संस्कृति खो रहा है।
“वह नई व्यवस्था सिर्फ लोगों को ही नहीं उनकी पहचान और उनकी पूरी संस्कृति को ही पुनर्वास
रहित विस्थापन की ओर धकेल रही है।” कंपनियाँ रूपी देवताओं को बॉक्साइट के वैध एवं
उससे कहीं अधिक अवैध खनन के लिए आदिवासियों की जमीन चाहिए। इनके अलावा इनके ही
क्षेत्र एवं इसके आसपास के बड़े-बड़े जोतदार आदिवासियों की ज़मीन हथिया लेने की फिराक
में होते है। बदलते हुए समय के ये देवता इतने निर्दय व खूंखार है कि ज़मीन हथियाने
के लिए खून-खराबे तक का सहारा लेते हैं। मरने वालों को नक्सलियों में खपा देते है।
खदान मालिकों एवं इनके दलालों द्वारा खनन हेतु जमीन को सस्ते भाव में हथिया लेना।
सरकारी लीज की भूमि पर कम लेकिन असुरों की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा खनन “छोटे-बड़े
सभी खदान-मालिको का एक ही रवैया। लीज की भूमि पर कम-वन विभाग, गैर मजरूआ
जमीन, असुर रैयत की जमीन से ज्यादा खनन किया करके अवैध खनन खुले
आम और वर्षो से जारी था।“13
आदिवासी क्षेत्र से जाने वाला बॉक्साइट जहाँ प्रोसेस होकर
अल्युमिनियम में गलता है यह जगह है- सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया। इस जगह और आदिवासियों
के जीवन में कितनी बड़ी भेद रेखा है। उभय की तुलना उपन्यास में रुमझुम की जबानी-‘‘हमारा बॉक्साइट यहाँ से डेढ़-दो-सौ
किलोमीटर दूर जहाँ प्रोसेस होकर अल्युमिनियम में ढ़लता है। वह जगह सिल्वर सिटी ऑफ
इंडिया कहलाती है – फूलों पार्कों से लदी हरी-भरी खूबसूरत कॉलोनी। एक से एक स्कूल,
चम-चमाते, बाजार, क्लब घर, योगा केन्द्र, लाइब्रेरी, खेल के मैदान और न जाने
क्या-क्या ! सुन्दर-सुन्दर कुत्तों को घुमाती सुन्दर महिलाएँ, बर्फ के गोलों से
गुलथुल उजले-उजले बच्चे, रंग-बिरंगी गाड़ियाँ। लगा इन्द्रलोक धरती पर उतर आया हो
और यहाँ पाट में- पानी और जलावन जुटाने में ही हमारी औरतों की आधी जिन्दगी गुजर
जाती है। बरसात के गिजंन की तो मत पूछिये। बन्द खदान के सैकड़ों गड्ढे विशाल
पोखरों में बदल जाते हैं। कीचड़ में लोटते सुअरों और हमारे बच्चों में फर्क करना
मुश्किल हो जाता है। वहाँ के गेस्ट हाउस के मेस में छत्तीस तरह के व्यंजन। मुहावरे
वाले नहीं, सचमुच के। क्या खाएँ-क्या नहीं खाएँ। एक ही दिन में पेट खराब हो गया।
यहाँ मकई का भुट्टा खा-खाकर जीभ पर घट्टा पड़ जाता है। हमारे ज्यादातर घरों में
भात-दाल सब्जी भई पर्व-त्यौहार का भोजन है।’’14
आदिवासियों को उनके निवास
स्थलों से हटाकर इनकी जमीन पर सरकार की ओर से बनाये गए बड़े-बड़े स्कूल जो
अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। लगता है इससे इस समाज में शिक्षा का
प्रचार-प्रसार होगा और इस समाज की दशा में सुखद बदलाव आएगा, किंतु प्रश्न यह है कि
क्या वास्तव में इस तरह के स्कूलों में दरिद्र आदिवासी समाज में लोगों को लाभ
मिलता है ? सुखी संपन्न परिवारों के बच्चों को तो ऐसे स्कूलों में प्रवेश मिलता है
किंतु पिछड़ा वर्ग इस तरह के स्कूलों में अध्ययन व अध्यापन के लाभ से वंचित रहता
है। इसी स्थिति का एक उदाहरण उपन्यास में है- पाथरपाट का आलिशान स्कूल। इसे लेकर
असुर रुमझुम की चिन्ता देखिए- ‘‘असुरों के
सौ से ज्यादा घरों को उजाड़कर बना था यह स्कूल। अभी भी आसपास असुर आबादी है।
ज्यादा दूर नहीं; बीस बाईस किलोमीटर के दायरे में लगभग सारी की सारी असुर,
बिरजिया, कोरवा आबादी बसती है। पिछले तीस वर्षों का रजिस्टर उठाकर देख लिजिए जो एक
भी आदिमजाति परिवार के बच्चे ने इस स्कूल में पढ़ाई की हो। मैंने खुद कितनी कोशिश
की थी। पिछले दो-तीन वर्षों से कैजुअल शिक्षक के रूप में काम करने की इच्छा है।
लेकिन वहाँ भी दाल नहीं गलती। आखिर हमारी छाया से भी क्यों चिढ़ते है ये लोग ?
माड-भात खिलाकर, अनपढ़ शिक्षकों के भरोसे, फुसलाकर स्कूल के हमारे बच्चे ज्यादा से
ज्यादा स्किल्ड लेबर पिंऊन, क्लर्क बनेंगे, और क्या ? यही हमारी औकात है। हमारी ही
छाती पर ताजमहल जैसा स्कूल खड़ा कर हमारी हैसियत समझाना चाहते हैं लोग।’’
पाथरपट के
स्कूल के सामने भौंरापट के आदिवासी लड़कियों के आवासीय स्कूल की स्थिति कितनी बदतर
है – “भौंरापाट का स्कूल सूअर का बखार नजर आता है। आधी-अधूरी बिल्डिंग, जैसे-तैसे
बना हॉस्टल, मुर्गीखानों जैसे शिक्षक –आवास। यहाँ साफ-सफाई होनी चाहिए
वहाँ सबसे ज्यादा गन्दगी , बच्चियों के मेस में
कभी-कभी झाड़ू पोंछा लगना भी था कि नहीं। कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं।” कुल
मिलाकर इस क्षेत्र में भी सुख सुविधाएँ है वह इस स्थानीय असुर समुदाय के लिए नहीं
है।
आदिवासी स्त्रियों के यौन-शोषण का जिक्र उपन्यास में हुआ है।
रणेन्द्र ने इस शोषण को एक मार्मिक लोकगीत के माध्यम से प्रकट किया है। “खदान के
मेठ-मुंशी, क्लर्क, अफसरों की डेरों में खटने
वाली असुर युवतियों पर रुपये-पैसे के लोभ के कुल जाति का नाम डुबोने का आरोप इस
गीत में लगाया जा रहा है किन्तु इसके साथ-साथ लड़कियों के इस तरह के काम करने के
लिए विवश करनेवाले कारणों की पड़ताल भी हुई है –
“काठी बेचे गेले
असुरिन
बाँस बेचे
गेलेगे,
मेठ संगे नजर
मिलयले,
मुंशी संग लासा
लगयले गे,
कचिया लोभे कुला
डुबाले
रुपया लोभे जात
डुबाले गे।”16
इस गीत में अनैतिक कार्य से जुड़ी युवतियों की भत्सर्ना की गई।
इनके प्रति समाज की शिकायत दर्ज हुई है। किन्तु असलियत यह है की वह महज शिकायत
नहीं बल्कि इसके साथ इस समाज की व्यथा एवं विवशता भी प्रकट होती है। “अन्दर से बुरी
तरह टूट चुके समाज का विलाप भूख और गरीबी ने अन्दर से इतना खोखला कर दिया है कि
सामाजिक व्यवस्था भरभरा गई है। अखाड़ा में बैगा-पाहन पुजार और गाँव के बड़े-बूढ़ों की
बात का वजन दिन-पर-दिनघटता जा रहा है। ठीक ही बात है कि घर में तीन-चार माह से
ज्यादा का अनाज नहीं हो तो कौन बेटों को गाँव छोड़ने और बेटियों को डेरा में काम के
बहाने रखनी बनाने से रोक सकता है ?16
रणेन्द्र की इस रचना में आद्यंत आदिवासी समाज की व्यथा का गान
सुनाई देता है। इस समाज की करूण कथा को बड़ी संजीदगी से लेखकने प्रस्तुत किया है।
उपन्यास में से उद्धृत निम्न गीत इस उपन्यास की मूल संवेदना को बखूबी बयाँ करता है –
“हमारी रात/भरपूर काली रात
होने का
आश्वासन दे रही है / उदास
....हवाएँ/ दूर कहीं विलाप कर रही
एक ज़ख्मी हिरण/ अपनी पीछे
आते हुए। शिकारी की आवाज़ सुनकर अपने आपको/ अपनी पूर्ण मृत्यु के लिए तैयार कर रहा
है
अपनी पूर्ण
मृत्यु............................... ।”17
सरकार की
और से भेड़िया अभयारण्य के बहाने असुरों के सैंतीस गाँव खाली कराने की नोटिस दी
जाती है। सरकार को जिन्दा मनुष्यों से ज्यादा भेड़ियों की चिन्ता है। “भेड़िया मन के
बचावे का आदमीमन के जान लैबें।” मजे की बात तो यह है कि इस अभयारण्य के लिए कंटीले
तारों का घेरा बनाने जैसा काम ‘वेदांग’ जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय
कंपनी को सौंपा जाता है। इसके पीछे सरकार एवं कंपनी दोनों की असली योजना कुछ और ही
है। बहुत वर्षों से इस इलाके से बॉक्साइट बाहर नहीं भेजकर यहीं कारख़ाना खोलेने की
बात उठती रही है। लगता है वेदांग उसी टोह में आ रहा है।”
इस असलियत को भल-भाँति समझने वाले असुरों द्वारा भेड़िया
अभयारण्य वाली योजना का विरोध किया जाता है। प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा जाता
है।
सत्ता और समृद्धि के सिंहासन पर विराजमान वर्ग के अन्याय-अत्याचार
से पीड़ित इस आदिवासी समाज की विस्थापन, स्त्रियों का यौन शोषण, खत्म होता
पारंपरिक व्यवसाय जैसी तकलीफ़ों और इनसे कुछ हद तक मुक्ति पाने की उम्मीद के साथ रुमझुम
असुर का प्रधानमंत्री को लिखा पत्र पाठक
के मर्म को छूए बिना नहीं रहता - “हमारी बेटियों और हमारी भूमि हमारे हाथों से
निकलती जा रही है। हम यहाँ से कहाँ जाएँगे ? यह हमारी
समझ में नहीं आ रहा। सच कहें तो हम बिना चेहरे वाले इन्सान होकर जीना नहीं चाहते।
हमें बचा लीजिए श्रीमान। हमारी आखरी आस आप ही है।” इस पत्र से सकारात्मक परिणाम न
मिलने पर आखिरकार संघर्ष का मार्ग अपनाया जाता है। आंदोलनकारियों द्वारा तीस-चालीस
खदानों में काम पर रोक लगा दी जाती है जिससे ग्लोबल देवताओं में खलबली मच जातीहै।
फिर आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी, प्रलोभन,
ब्लेकमेलिंग, छल, हत्या,
आदिवासियों के लिए विकास के नये पैकेज के प्रसंग आते हैं। उपन्यास के अन्त में एक
कंपनी द्वारा की जा रही घेरेबंदी के खिलाफ बातचीत के लिए जाते वक्त जमीन में उनके द्वारा
बिछाये गए लैंड माइन्स की चपेट में आकर आंदोलनकारियों की धज्जियाँ उड़ जाने और
राजधानी के यूनिवर्सिटी हॉस्टल से सुनील असुर के अपने साथियों के साथ लड़ाई की
बागडोर संभालने के लिए निकलने के प्रसंग है।”18
असुर समाज के संकट व संघर्ष के साथ-साथ इस समाज की संस्कृति
को भी लेखक ने चित्रित किया है। आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक व
सांस्कृतिक जीवन के विविध पहलुओं का वर्णन उपन्यास में जगह-जगह पर हुआ है।
“रणेन्द्र अपनी इस कृति में असुर समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षों को उजागर
करते हैं। यह प्रकृतिपूजक समाज है, इसलिए इसके सदस्यों में
चट्टान की दृढ़ता, नदी की तरलता और हवा की गति की एकता मिलती है। यह भेदभाव से रहित समतावादी समाज है। असुरों के
प्रत्येक गाँव के बीच में स्थित अखाड़े में गुरुवार के दिन सारे बुजुर्ग, समझदार ,सयाने
बैठकर गाँव-घर-समाज की समस्याओं पर विचार करते हैं। इन बैठकों में स्त्रियाँ भी
उपस्थित रहती है। अखाड़ा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। इस समाज
में स्त्री-पुरुष के बीच समानता है। महिलाओं को ‘सियानी’ कहा जाता
है, ज़नानी नहीं। ‘सियानी’ शब्द उनकी
समझदारी की और इंगित करता है जबकि ज़नानी’ शब्द प्रजनन से जुड़कर उनके
व्यक्तित्व को सीमित करता है। नर-नारी का प्रेम वहाँ दण्डनीय अपराध नहीं है। नगरों
में ‘लिविंग टूगेदर’ का जो चलन शुरू हुआ है, वह आदिवासी
समाज में पहले से ही मान्य है। संगीत और नृत्य इस समाज की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसके
माध्यम से नर-नारी के बीच राग-भाव तथा प्रकृति और जीवन के प्रति तीव्र प्रेम की
अभिव्यक्ति होती है।”19
ज़्यादातर संयुक्त परिवार में रहने वाले इन लोगों का जीवन
निर्वाह खेती, खान-खदान में मजदूरी एवं जंगली पैदाशों के सहारे होता है।
“पूरे इलाके के गाँवो में दो-चार परिवार के छोड़कर अधिकांश परिवारों को पास इतनी
जमीन नहीं थी कि वह अपने जीवन-निर्वाह के लिए साल भर का अनाज उगा सके। अत: वे खान-खदान
में काम करके या फिर जंगल पर ही निर्भर रहते, महुआ, कटहल कई
तरह के कन्द और साग सब पेट भरने के काम आते हैं। इसके साथ पशुपालन भी इनकी आजीविका
का महत्वपूर्ण साधन रहा है – मिट्टी के घरों के आँगन के एक कोने में लम्बा सा
गोदाम, बरामदे में मुर्गियों के भी बाड़े “ये गाय-गोरू, बकरी-छगरी, मुर्गी, सूअर केवल पशु नहीं थे बल्कि आदिवासियों के पासबुक भी थे। हारी-बीमार, शादी-ब्याह
इन्हीं के भरोसे, जब भी जरूरत होती, बेचारे मूक
प्राणी हाट पहुँचा दिये जाते।”
घर की साज-सजावट,
लीपने-पोतने में स्त्रियों का गृहकला कौशल दिखता है “घर की दीवारों को बड़े जतन से
महिलाएँ लीपती थीं। महिलाओं को यह पता रहता था कि घर लीपने वाली काली,
पीली और सफ़ेद मिट्टियाँ कहाँ मिलती थी...... दीवारें पहले काली मिट्टी से लीपी
जातीं। दीवारों पर काली मिट्टी के लेप सुखाने के बाद उन पर सफ़ेद मिट्टी का लेप
चढ़ाया जाता। फिर पूरी हथेलियों को नचा-नचाकर एक वृत्ताकार आकृति उभारी जाती। जिनमें
उनकी हथेलियों की छाप झलक मारती। यह अद्भूत हथेलियों की छाप वाले चित्र न केवल घरों-दीवार
पर बल्कि खेतों-खलिहानों,
जंगल-बगानों
खानों, नदी-नालों,
सोता,
झरनों
में हर कहीं दिखाई देते।
पर्व-त्यौहार
पर स्त्री-पुरुष
अपने दुःख-दर्द
को भुलाकर आनंद-उल्लास
से नाच-गाने में शामिल होते हैं - “अखाड़े
में पर्व-त्यौहार
सरहुल, हरियारी,
सोहराय
पर रातभर मांदर बजता। रातभर गाँव-गाँव
से जवान लड़के जुड़ते। लड़कियाँ जुड़ती। मदुरा के बोलों पर रात भर चाँद नाचता। सखुआ
और पलाश नाचता। नदी-झरना
पहाड़ नाचते। एक साथ पूरी प्रकृति नाचती।”
विविध अवसरों पर इन आदिवासी स्त्री-पुरुषों
द्वारा गाये जाने वाले गीतों में इनकी सुखद व दुखद अनुभूतियाँ प्रकट होती है। देवर-भाभी
के रिश्ते में भाभी की देवर के प्रति प्रकट होने वाली भावना निम्न देवर गीत में देखिए
–
“काहे
रे देवरा मन तोरा कुम्हले
काहे
रे मन सूखी गेला रे,
भूखे
रे देवरा मन तोरा कुम्हले
पिया
से मन सूखी गेला रे।”20
विविध अन्धविश्वास,
टोना-टोटका
भी इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। उपन्यास के प्रारंभ में मुड़ी कटवा जैसे अंधविश्वास
का जिक्र है- “एक
अन्धविश्वास है इलाके में हालाँकि अब बहुत घट गया है। लेकिन अभी भी खरीफ के सीजन में
दो-चार घटनाएँ घट ही जाती
है। आदमी के जान की तो मानो कोई कीमत ही नहीं....
दरअसल
अब भी कुछ लोगों के मने में यह बात बैठी हुई....है
कि धान को आदमी के खून में सानकर बिचड़ा डालने से फसल बहुत अच्छी होती है। इसीलिए इस
सीजन में मुड़ीकटवा घूमते रहते हैं।” देवी-देवताओं
को प्रसन्न करने एवं इनकी कृपा पाने के लिए पशु की बलि चढ़ाना या आदमी के खून से तिलक
करना जैसे अन्धविश्वासों के प्रमाण उपन्यास में मिलते हैं -
“देवी को जब बलि की जरूरत महसूस होती है तो वहाँ से
नगाड़े की आवाज सुनाई देती है।” एतवारी
के आदमी गन्दूर के नाम की कहानी में एक टोटके का उल्लेख हुआ है।
“गन्दूर के पहले पैदा हुए भाई-बहन
नहीं बचते थे। जन्म लेने के कुछ दिन-महिने
में गुजर जाते। गन्दूर के जन्म के समय टोटका किया गया। गन्दूर की आजी
(दादी) ने
उसे कपड़े में लपेटा और घर के अहाते के बाहर कूड़े के ढ़ेर पर धर दिया। थोड़ी देर बाद
वापस लायी। बच्चा इस बार बच गया। कूड़ा का ढेर यहाँ गन्दूर कहा जाता है सो इनका नाम
गन्दूर पड़ गया। ”
संदर्भ
1.
साहित्य के आईने आदिवासी विमर्श – सं.डॉ.एम.फिरोज खान, डॉ.शगुफ्ता नियाज, पृ.
136
2.
आदिवासी साहित्य दशा एवं दिशा – सं.डॉ.एम. फिरोज खान, डॉ.शगुफ्ता नियाज, पृ.
11.
3.
ग्लोबल गाँव के देवता : समूल विनाश की आहट सुनने की कोशिश- रणेन्द्र, अन्यथा,
अंक-16 पृ.62
4.
नया सुर-असुर संग्राम – पुष्पपालसिंह, इंडिया टूडे, 24 मार्च 2010, पृ. 63
5.
आदिवासी साहित्य- सं- डॉ. खाननाप्रसाद अमीन, पृ.263
6.
ग्लोबल गाँव के देवता- रणेन्द्र, पृ.11
7.
वही, पृ.12
8.
आदिवासियों के प्रति सुनियोजित साजिश और ग्लोबल गाँव के देवता-मुकेश कुमारी, नव
निकष, मार्च 2015, पृ.65
9.
ग्लोबल गाँव के देवता, पृ.83
10.
21वीं शती का हिन्दी उपन्यास- पुष्पपाल सिंह, पृ.365
11.
ग्लोबल गाँव के देवता, पृ.13
12.
वही, पृ.14
13.
वही, पृ.27
14.
वही, पृ.16-17
15.
वही, पृ.38
16.
वही, पृ.39
17.
वही, पृ.90-91
18.
असुरों का संकट और संघर्ष - सुधीर सुमन. पृ.68-69
19. अनहद, वर्ष-1, अंक-1, जनवरी-2011, पृ.132
20. ग्लोबल गाँव के देवता, पृ. 25-26
डॉ. हसमुख परमार
एसोसिएट प्रोफ़ेसर
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग
सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर
जिला- आणंद (गुजरात) – 388120


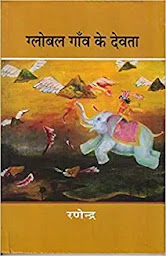


पढ़ते समय यह प्रतित हुआ गोया हम उनके बिच में हैं।
जवाब देंहटाएंअत्यंत सुंदर प्रस्तुति।
खालिद
आदरणीय सर जोहार !
जवाब देंहटाएंबहुत बहुत आभार सर आपका...आपने ' 9 अगस्त,आदिवासी दिवस' को ' शब्द सृष्टि ' में शामिल किया और इसी दिवस को ध्यान में रखते हुएँ आदिवासी जीवन, प्रकृति, समाज और उनके संकट की पहचान करवानेवाले, साहित्य की कड़ी में महत्वपूर्ण ऐसे रणेन्द्र जी के उपन्यास 'ग्लोबल गाँव के देवता' पर सुंदर आलेख की प्रस्तुति की जो आदिवासी अस्मिता के संकट को अभिव्यक्त करता है ।
ખૂબ સરસ સાહેબ આદિવાસી સમાજ વિશે આટલું ઉંડાણ પૂર્વકની માહિતી આપવા બદલ આખો લેખ એક જ બેઠકે વાંચી નાખ્યો...
जवाब देंहटाएंआदिवासी समाज के प्राण- प्रश्नों को बड़ी संजीदगी से व्यक्त करते उपन्यास की स्तरीय और सटीक समीक्षा...
जवाब देंहटाएंहार्दिक शुभकामनाएं🙏💐
जोहर
जवाब देंहटाएंआदिवासी समाज के संकट, संघर्ष एवं संस्कृति की महागाथा : 'ग्लोबल गाँव के देवता'पर सुंदर आलेख की प्रस्तुति की सर
हार्दिक शुभकामनाएं💐💐💐
अत्यंत सुंदर प्रस्तुति
जवाब देंहटाएंआदिवासी जीवन, प्रकृति, समाज और उनके संकट की पहचान करवानेवाले, साहित्य की कड़ी में महत्वपूर्ण ऐसे रणेन्द्र जी के उपन्यास 'ग्लोबल गाँव के देवता' पर सुंदर आलेख की प्रस्तुति की जो आदिवासी अस्मिता के संकट को अभिव्यक्त करता है ।हार्दिक शुभकामनाएं💐💐💐
जवाब देंहटाएंआदिवासी जीवन सम्बन्धित उत्तम प्रस्तुति।
जवाब देंहटाएंहार्दिक शुभकामनाएं 🙏🙏
मोनिका प्रजापति
बधाई आदरणीय , आपका आलेख विशिष्ट संस्कृति का परिचय देते हुए 'ग्लोबल गाँव के देवता' उपन्यास को पढ़ने की सम्यक दृष्टि प्रदान करता है , पढ़ने की जिज्ञासा जगाता है ।
जवाब देंहटाएंसादर नमन 💐🌷